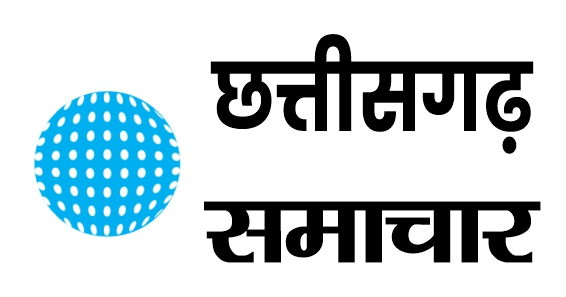श्रीमद भगवत गीता हजारो वर्षो से हम मानवो का बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के हमारा मार्गदर्शन कर रही है, ये केवल सनातन धर्म की धार्मिक किताब नही अपितु जीवन जीने का विज्ञान और व्यक्तीत्व निर्माण का विज्ञान स्वयं ईश्वर द्वारा दिया हुआ है । प्रथम दृष्टया हम देखते है तो यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रतीत होती है । पर ध्यान से देखने पर और चिंतन करने पर हमारे ध्यान में आता है, कि इसमें मानव जीवन की सभी समस्याओं का निवारण और और अवसाद जिससे आजकल की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रसित है । उसका भी समाधान बताया है, इसमें में कोई भक्ति और धर्म की बात नही करुगा क्योकि ये दोनों विषय अंतर आत्मा के है, में सिर्फ उन श्लोकों की बात करूँगा जो आज के परिपेक्ष्य में युवाओ के लिए उपयोगी व मार्गदर्शक है । क्योकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस विज्ञान को केवल अर्जुन या संजय को सुनाने के लिए तो कहा नही होगा उनका उद्देश्य तो सम्पूर्ण मानव जाति को ये विज्ञान प्रदान कर उसका कल्याण था । अर्जुन भी अवसाद (Depression) व कुंठा का शिकार हो गया था फिर भगवान ने उसे भी अवसाद से निकाला था कैसे यही भगवद गीता सुनाके क्योकि ये कोई साधारण वार्तालाप नही था ये स्वयं ईश्वर जीवन जीने का विज्ञान हम मानवो को दे रहे थे । इस विज्ञान से हम केवल कुंठा व अवसाद से ही नही निकल सकते अपितु अपने जीवन को इस मार्ग पर चलाकर सफल कर सकते है । विश्व के कई देशों के विश्वविद्यालयो व शोध संस्थानों में हमारे इसी वैज्ञानिक ग्रन्थ पर शोध चल रहा है । कई विद्वानों ने इसके ऊपर टिका या अपनी सरल भाषा में अनुवाद लिखे है । में भी प्रथम अध्याय से जो श्लोक युवापीढ़ी के लिए उपयोगी व मार्गदर्शक है । वो बताउगा इस विज्ञान में कुल 18 अध्याय में 700 श्लोक है, हर अध्याय का अपना एक अलग नाम और शिक्षा है । जिसमे स्वयं ईश्वर हम मानवो को भक्तियोग, कर्मयोग, मुक्तिमार्ग, ध्यानयोग, व्यक्तीत्व निर्माण आदि अनन्त ज्ञान दे रहे है । वैसे तो इस विज्ञान के हर एक श्लोक पर एक पुस्तक लिखी जा सकती है और स्वयं शेष और महेश भी योगेश्वर के सम्पूर्ण ज्ञान और चरित्र का वर्णन करने में स्वयं को समर्थ नही पाते है । जैसा स्वयं भगवान शिव ने पद्मपुराण में स्पष्ट किया है । क्योकि विज्ञान में कई शाखाएं होती है आप सम्पूर्ण विज्ञान के ज्ञाता ना होकर किसी एक शाखा के ज्ञाता हो सकते है । या जो आपके लिए उपयोगी हो वही ग्रहण करके बाकी छोड़ देते है, मेने भी जो युवाओ के लिए उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान के श्लोक है वही बताने का प्रयास किया है । तो प्रथम अध्याय से शुरू करते है ये विज्ञान :
-
अध्याय 1 : कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में निरीक्षण का व्यवहारिक ज्ञान
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्॥
कृपया परयाविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत्।
उन उपस्थित सम्पूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। श्लोक 27
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक से स्पष्ठ है, अर्जुन वीर व ज्ञानी होते हुए मोह से ग्रसित हो जाते है, उन स्वजनों के लिए जो उन्हें नष्ट करने के लिए आये थे, हम भी अपने जीवन में कष्ट या दुःख अत्यधिक मोह के कारण पाते है आप स्वयं मनन कीजियेगा ।
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ श्लोक 30
हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ ।
व्यवहारिक अर्थ : हमारे अधिकतर दुःखों के मूल या जड़ में ज्यादा मोह (लगाव) होता है । अर्जुन की स्थिति अत्यधिक मोह के कारण श्लोक से स्पष्ट है ।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥ श्लोक 31
हे केशव! मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन-समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता ।
व्यवहारिक अर्थ : हमारे जीवन मे भी हम सत्य अत्यधिक मोह के कारण नही देख पाते और सफलता, कल्याण के लक्षण हमे विपरीत या उल्टे दिखते है ।
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च।
किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा॥ श्लोक 32
हे कृष्ण! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद! हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है?
व्यवहारिक अर्थ : कई बार हमारा अज्ञान जनित मोह (लगाव) हमसे हमारी विजय, सफलता और सुख को हमसे दूर ले जाता है । श्लोक में अर्जुन स्वयं बता रहे है अतः हमें इससे बचना चाहिए
एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्।
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः॥ श्लोक 47
संजय बोले- रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुष को त्यागकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए ।
व्यवहारिक अर्थ : कई बार हमारा मोह (लगाव) इतना अधिक होता है कि रणभूमि या कर्म क्षेत्र से भी हमे दूर कर देता और हम अपने अस्त्र या अपने कर्मो का त्याग कर अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर इसी तरह थककर, हारकर बैठ जाते है ।
-
अध्याय : 2 गीता का सार का व्यवहारिक ज्ञान
श्रीभगवानुवाच
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्।
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्ति
श्रीभगवान बोले- हे अर्जुन! तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है ।
व्यवहारिक अर्थ : भगवान स्वयं कहते है, की असमय मोह (लगाव) श्रेष्ठ मनुष्य या बुद्दिमान मनुष्यो के लिए नही है, यह स्वर्ग या वर्तमान परिपेक्ष में सफलता ये भी आज के समय स्वर्ग है, स्वर्ग कोई जगह नही बल्कि मनोदशा है जहाँ आप आनन्दित हो और यह मोह कीर्ति (Fame) को नष्ट करता है ।
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥ श्लोक 3
इसलिए हे अर्जुन! नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप! हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा ।
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक में भगवान अर्जुन या हम मानवो से कह रहे है नपुंसकता या कर्महीनता को प्राप्त मत हो और युद्ध के लिए या कर्म करने के लिए तैयार हो जा कई बार हम कर्म या प्रयत्न करना छोड़ देते है लक्ष्य के लिए जो उचित नही ।
श्री भगवानुवाच
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे।
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ श्लोक 11
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन! तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पण्डितों के से वचनों को कहता है, परन्तु जिनके प्राण चले गए हैं, उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पण्डितजन शोक नहीं करते ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान अत्यंत व्यवहारिक बात कह रहे है, एक बात हम सभी जानते है जिसने जन्म लिया है । वो अपना जीवन जीके एक दिन इस दुनिया से जाएगा इससे कोई नही बच सकता पर हम कई बार सच को देखने की बजाय अत्यधिक दुःख और अवसाद में चले जाते है, जो पंडितजन या बुद्धिमानो के लिए भगवान ठीक नही बताते ।
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति॥ श्लोक 13
जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भी भगवान समझा रहे है हम सब के पास निश्चित समय बचपन, जवानी और वृद्धावस्था और अंत में संसार से जाना इसमें धीर बुद्दिमान लोग मोहित नही होते ।
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्
हे कुंतीपुत्र! सर्दी-गर्मी और सुख-दुःख को देने वाले इन्द्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत! उनको तू सहन कर ।
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे है सर्दी-गर्मी और सुख-दुःख इंद्रियों और विषयो यानी के संयोग या व्यवहारिक अर्थो में संसार और उससे होने वाली परेशानियां आएगी ही इसलिए इनको सहने वाले बनो श्लोक में महत्वपूर्ण बात अर्जुन को भगवान ने भारत कहा भारत कौन? भारत यानी हम सब ।
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ।
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥ श्लोक 15
क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ! दुःख-सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इन्द्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है ।
व्यवहारिक अर्थ : भगवान कह रहे है दुःख-सुख को समान समझने वाले क्योकि जीवन में ये दोनों आएंगे इंद्रियों और विषय संयोग ये भी होंगे पर जो इनमें व्याकुल या परेशान नही होगा, वह मोक्ष या सफलता मोक्ष भी मेरे अनुसार मन स्थिति है, जहाँ कोई कष्ट या संकल्प, विकल्पों का अभाव हो ।
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ श्लोक 38
जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुख को समान समझकर, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा ।
व्यवहारिक अर्थ : जय – पराजय, लाभ – हानि और सुख – दुःख ये सब तो जीवन के अभिन्न अंग है । अतः हमें इन्हें समान समझकर
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाका ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्॥ श्लोक 41
हे अर्जुन! इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनन्त होती हैं ।
व्यवहारिक अर्थ : भगवान इस श्लोक में बता रहे है कर्म योग या जो आपका प्रोफेशन है, उसमे निश्चयात्मिका बुध्दि या किसी निश्चय पर पहुचने वाली बुध्दि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुध्दि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनन्त होती हैं ।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥ श्लोक 46
सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक अनुसार योगेश्वर ये कह रहे है सब और से परिपूर्ण जलाशय अर्थात बड़े तालाब के प्राप्त होने पर मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण या ज्ञानी का समस्त वेदों या ज्ञान में उतना ही प्रयोजन रहता है इसमें भगवान गीता को अनन्त ज्ञान स्वयं कह रहे है ।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥ श्लोक 47
तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो ।
नोट : ये श्लोक तो अत्यंत प्रसिद्ध है सभी बचपन से सुन रहे है व इसका अर्थ भी जानते है ।
योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥
श्लोक 48
हे धनंजय! तू आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धिवाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है ।
(जो कुछ भी कर्म किया जाए, उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ‘समत्व’ है।)
व्यवहारिक अर्थ : तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि (सफलता) और असिद्धि (असफलता) में समान बुद्धिवाला होकर योग या अपने काम मे स्थित हो मन लगा कर यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से सफलता और असफलता में एक समान रहने का कह रहे है ।
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः॥ श्लोक 49
इस समत्वरूप बुद्धियोग से सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय! तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूँढ अर्थात् बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यन्त दीन हैं ।
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक में भगवान बुद्धियोग याने दिमाग के इस्तेमाल की बात कह रहे है, हमारे दैनिक जीवन मे भी हम बुद्धियोग के प्रयोग के स्थान पर कुंठा या अवसाद कर लेते है । जबकि भगवान ने बुद्धियोग से रक्षा का उपाय करने की बात कही है ।
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥ श्लोक 53
भाँति-भाँति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा ।
व्यवहारिक अर्थ : भाँति-भाँति के वचनों को सुनकर अक्सर बुद्धि विचलित हो जाती है तब परमात्मा श्री कृष्ण कह रहे है कि योग या अपना काम करने के स्थिरबुद्धि अत्यंत आवश्यक है परमात्मा के साक्षात्कार और सफलता प्राप्ति के लिए स्थिर बुध्दि अत्यंत आवश्यक है ।
अर्जुन उवाच
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥
श्लोक 54
अर्जुन बोले- हे केशव! समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक में अर्जुन भगवान से समाधि में स्थित परमात्मा को या सफलता को प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि व्यक्ति के लक्षण वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है आदि पूछ रहे है ।
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥ श्लोक 56
दुःखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है ।
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक में भगवान स्थिर बुद्धि के लक्षण बता रहे है दुःखों की प्राप्ति पर जिसके मन मे उद्वेग या मन विचलित तथा सुख प्राप्ति में जिसका मन अनछुआ रहता है तथा जसको क्रोध (गुस्सा), राग या मोह और भय (डर ) जिसको प्रभावित नही करता वो स्थिरबुद्धि कहा जाता है ।
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्
नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ श्लोक 57
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान स्थिरबुद्धि मनुष्य के और भी लक्षण बता रहे है, जो स्नेहरहित हुआ व शुभ (अच्छा) प्राप्त होने पर ना जो खुश होता है व अशुभ (बुरा) प्राप्त न दुःख करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है ।
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्
और कछुवा सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियों के विषयों से इन्द्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिए) ।
व्यवहारिक अर्थ : स्थिरबुध्दि कैसे करना है इसकी विधि बता रहे है, भगवान जैसे कछुआ अपने सभी अंग सब और से समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी चाहिए इंद्रियों और उनके विषय जैसे काम, क्रोध, मोह, लालच से हटा कर पहले अपना दिमाग स्थिर करे क्योकि सफलता के लिए स्थिर दिमाग आवश्यक है ।
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ श्लोक 60
हे अर्जुन! आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इन्द्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं ।
व्यवहारिक अर्थ : आसक्ति (लगाव) का नाश ना होने से ये हमारी प्रमथन स्वभाव या चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों को जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हो उसके मन को भी बलात हर लेती हैं ।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ श्लोक 61
इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष की इन्द्रियाँ वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है ।
व्यवहारिक अर्थ : इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रभु बता रहे है जो मेरे चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान या (Meditation) में बैठे क्योकि जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है । यहाँ प्रभु बता रहे है स्थिर बुद्धि का महत्त्व हम सभी जानते भी है ।
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते।
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥श्लोक 62
विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है ।
व्यवहारिक अर्थ : विषयो का चिंतन अर्थात जो सांसारिक विषय या अन्य निजी विषय होते है । उनके बारे में सोचने से उनमे आसत्ति या लगाव हो जाता है, और उन विषयो को प्राप्त करने की इक्छा उत्पन्न होती है और जब उनमे कोई विघ्न या बाधा आती है तो क्रोध या गुस्सा आता है ।
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ श्लोक 63
क्रोध से अत्यन्त मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञानशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है ।
व्यवहारिक अर्थ : यहाँ भगवान क्रोध और उससे होने वाले नुकसान के विषय मे बता रहे है, क्रोध आने पर मूढ़ भाव या मूर्खता का भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति या हमारी चेतना में भृम हो जाता है, व बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि अर्थात अगर दिमाग का नाश होने पर जीव अपनी वर्तमान स्थिति से गिर जाता है ।
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ श्लोक 64
परंन्तु अपने अधीन किए हुए अन्तःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई, राग-द्वेष रहित इन्द्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अन्तःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है ।
व्यवहारिक अर्थ : यहां भगवान प्रसन्न या खुश रहने का तरीका बता रहे है,जिसका मन और राग-द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना अपने अधीन कर लेता है या अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वो प्रसन्न रहता है
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥ श्लोक 65
अन्तःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके सम्पूर्ण दुःखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है ।
व्यवहारिक अर्थ : भगवान ने बताया है इस श्लोक में की जिसका अन्तः करण या मन प्रसन्न होता है उसे सम्पूर्ण दुःखों का अभाव होता है और उस प्रसन्न चित वाले कर्मयोगी की बुद्धि सब तरफ से हटकर एक परमात्मा या जो सफलता चाहता है उनके लिए उनके लक्ष्य में लग जाती है ।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्॥ श्लोक 66
न जीते हुए मन और इन्द्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अन्तःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है?
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे है अगर हमारा मन और इंद्रियां स्वयं के द्वारा जीती ना गई हो तो फिर उस ना जीते हुए मन मे भावना नही होती और भावनाहीन मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती शान्ति रहित या अशान्त मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है ।
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥ श्लोक 67
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों में से मन जिस इन्द्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान सावधान कर रहे है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु अपने साथ बहाकर ले जाती है वैसे ही हमारा मन जिस इंद्री के साथ सबसे अधिक होता है वही हमारी बुद्धि या दिमाग हर या खराब करने के लिए पर्याप्त होगी ।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्
इसलिए हे महाबाहो! जिस पुरुष की इन्द्रियाँ इन्द्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है ।
व्यवहारिक अर्थ : भगवान अर्जुन से कह रहे है महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार निग्रह या वश में है, उसी का दिमाग स्थिर है
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं- समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥ श्लोक 70
जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान सागर या समुद्र का उदाहरण देकर समझा रहे है कि सारी नदियों का जल जैसे समुद्र को बिना विचलित किए हुए समा जाता है वैसे ही सब भोग स्थितप्रज्ञ पुरुष या स्थिर दिमाग जीव में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किये बिना समा जाते है, वही परम् शांति या सफलता को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नही
इस अध्याय में भगवान ने स्थिर बुद्धि या स्थिर दिमाग के महत्व को बताया है, जिसका महत्व सफलता के लिए हम सभी जानते है
-
अध्याय 3 : कर्म योग का व्यवहारिक ज्ञान
न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते।
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥ श्लोक 4
मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगनिष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्यागमात्र से सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठा को ही प्राप्त होता है । (जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम ‘निष्कर्मता’ है।)
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक से भगवान स्पष्ट कर रहे है, की कर्मो को आरम्भ किये बिना और कर्मों को त्याग या छोड़ देने से योगनिष्ठा या अपने काम के प्रति निष्ठा नही होती ।
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ श्लोक 5
निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान का स्पष्ट सन्देश है कि मनुष्य किसी भी काल मे 1 सेकेंड के लिए भी कर्म किये बिना नही रह सकता क्योंकि जितने भी मानव है वो मा प्रकृति के गुणों से मजबूर है वह या शारीरिक कर्म करेगा या मानसिक कर्म करेगा ।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ श्लोक 6
जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान ने पाखण्ड और आडम्बर पर प्रहार करते हुए स्पष्ट किया है कि जो मूढ़ बुद्धि या मूर्ख मनुष्य हठपूर्वक या जिद करके ऊपर से रोककर मन ही मन इंडियो के विषय काम, लोभ, मोह, आदि का चिंतन करता है वो मिथ्याचारी या ड्रामेबाज कहा जाता है हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हमको मिल जायेंगे ।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥ श्लोक 7
किन्तु हे अर्जुन! जो पुरुष मन से इन्द्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ।
व्यवहारिक अर्थ : इसमें भगवान बता रहे है मनुष्यो में कौन श्रेष्ठ या बड़ा है जो मन से इंद्रियों को वश करके अनासक्त हुआ या अलग होकर समस्त इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण या पूरे मन से अपने काम को करना आदि करता है वही श्रेष्ठ है ।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः॥ श्लोक 8
तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ।
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक अत्यंत व्यवहारिक है तू शास्त्रविहित या जो सिस्टम बना है उसके अनुसार कर्म या काम कर क्योकि कुछ ना करने से कुछ करना अति श्रेष्ठ है क्योकि कुछ ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नही होगा सीधे शब्दों में कहे तो अगर तू कुछ कमाएगा नही तो खायेगा क्या ।
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः॥ श्लोक 19
इसलिए तू निरन्तर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्यकर्म को भलीभाँति करता रह क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान निरन्तर कर्म करने की शिक्षा आसत्ति से या लगाव से रहित होकर करने की दे रहे है क्योंकि आसत्ति से रहित मनुष्य कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को चाहने वाला परमात्मा को और सफलता चाहने वाला सफलता को प्राप्त होगा ये भी अत्यंत व्यवहारिक बात है ।
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ श्लोक 21
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है (यहाँ क्रिया में एकवचन है, परन्तु ‘लोक’ शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी ।
व्यवहारिक अर्थ : आज के परिपेक्ष्य में महत्वपूर्ण श्लोक श्रेष्ठ मनुष्य या आदरणीय, पूजनीय उनके द्वारा जैसा आचरण या व्यवहार किया जाएगा अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा पाकर वैसा ही व्यवहार करेगे ये श्लोक माता- पिता, गुरुजन और सभी पूजनीयों के लिए महत्वपूर्ण है।
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽति कर्मभिः॥ श्लोक 31
जो कोई मनुष्य दोषदृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान कह रहे है जो मनुष्य दोषदृष्टि से रहित या भगवान में विश्वाश करके उनके इस मत या व्यवहारिक विज्ञान का अनुसरण करते है वो समस्त बन्धनों से छूट जाते है अब बंधन सांसारिक भी तो होते है ।
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥ श्लोक 32
परन्तु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू सम्पूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ ।
व्यवहारिक अर्थ : ये श्लोक में चेतावनी है समस्त मानवो के लिए जो मनुष्य मुझमे दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत या मेरे द्वारा दिये हुए विज्ञान के अनुसार नही चलते है, तो उन मूर्खों को तू सम्पूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ ।
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ॥ श्लोक 34
इन्द्रिय-इन्द्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इन्द्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान् शत्रु हैं ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान कह रहे है हमारी हर इंद्री में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं । मनुष्य को उन दोनों के वश में नही होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण या सफलता मार्ग में विघ्न या बाधा करने वाले महान शत्रु हैं ।
धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥ श्लोक 38
जिस प्रकार धुएँ से अग्नि और मैल से दर्पण ढँका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढँका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढँका रहता है ।
व्यवहारिक अर्थ : श्लोक में योगेश्वर कह रहे है जैसे धुंए से अग्नि और मैल से दर्पण ढँका रहता है, जेर से गर्भ वैसे ही उस काम या भौतिक इक्छाओ द्वारा ये यह ज्ञान ढँका रहता है । ये अग्नि, दर्पण, गर्भ उदाहरण देकर भगवान समझा रहे है कि किस प्रकार सांसारिक आकांक्षाओ द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढँका रहता है ।
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥ श्लोक 39
और हे अर्जुन! इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढँका हुआ है ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में काम या भौतिक इक्छाओ को योगेश्वर ने अग्नि के समान कभी न पूर्ण या तृप्त होने वाला बताया व इसे ज्ञानियों का नित्य वैरी बताया है इसी से ज्ञान ढँका हुआ है ।
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्॥ श्लोक 40
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि- ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है।
व्यवहारिक अर्थ : काम या भौतिक इक्छाओ के निवास किसे कहा है योगेश्वर ने तो मन, इंद्रियों, बुद्धि ये सब इसके वास् स्थान है यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है । मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्पूर्ण श्लोक
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्॥ श्लोक 41
इसलिए हे अर्जुन! तू पहले इन्द्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल ।
व्यवहारिक अर्थ :श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे है तू पहले इंद्रियों वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल । इस श्लोक में प्रभु ने स्वयं इस गीता ज्ञान को विज्ञान कहा है
इस ध्याय भगवान ने इंद्रियों और बुद्धि, मन को नियंत्रण की महत्वता बताई है जिसका महत्व हम सभी जानते है।
-
अध्याय 4 : दिव्यज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्॥ श्लोक 21
जिसका अंतःकरण और इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर-संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता ।
व्यवहारिक अर्थ : महत्वपूर्ण व्यवहारिक श्लोक जिसका अंतः करण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा अशारहित पुरुष केवल शरीर-सम्बन्धी कर्म करता हुआ पापो को प्राप्त नही होता श्लोक का अर्थ कांच की तरह ही व्यवहारिक व पारदर्शी है ।
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञा
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ श्लोक 33
हे परंतप अर्जुन! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में भगवान ज्ञान यज्ञ या ज्ञान प्राप्ति के लिए किए गए परिश्रम को अन्य किसी भी यज्ञ से श्रेष्ठ बता रहे है । सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते है ।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः॥ श्लोक 34
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भलीभाँति दण्डवत् प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभाँति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में योगेश्वर गुरुजनों के प्रति व्हवहार और उनके महत्व की शिक्षा दे रहे है उन्हें दण्डवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भलीभाँति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश देंगे ।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि॥ श्लोक 36
यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह सम्पूर्ण पाप-समुद्र से भलीभाँति तर जाएगा ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में प्रभु कृष्ण कह रहे है, की अगर तू सब पापियों से अधिक पाप करने वाला भी हो तो भी तू ज्ञान रूप नाव द्वारा नि:सन्देह सम्पूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा । श्लोक में भगवान ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुते
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ श्लोक 37
क्योंकि हे अर्जुन! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है।
व्यवहारिक अर्थ :ज्ञान की महत्वता पुनः प्रतिपादित करते हुए भगवान कहते है जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है । ज्ञान की शक्ति बताई है प्रभु ने
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ श्लोक 38
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मा में पा लेता है ।
व्यवहारिक अर्थ : ज्ञान को भगवान ने संसार मे सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला कहा है और उस ज्ञान को मनुष्य कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धान्त: करण करता हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है । इस श्लोक में भगवान ज्ञान की महत्वता और शुद्धान्: करण या साफ मन कि बात कही है जो व्यवहारिक है ।
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्धवा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ श्लोक 39
जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलम्ब के- तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है ।
व्यवहारिक अर्थ : भगवान इस श्लोक में बता रहे है ज्ञान किसे प्राप्त होता है जितेंद्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शांति या सफलता को प्राप्त हो जाता है आप जानते है सफलता प्राप्ति में ज्ञान का महत्व
अज्ञश्चश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ श्लोक 40
विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है ।
व्यवहारिक अर्थ : विवेकहीन और श्रद्धारहित मनुष्य परमार्थ से अवश्य भृष्ट हो जाता है । ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है । इस श्लोक का एक एक शब्द पारदर्शी है ।
इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान का महत्व बताया है हर सफलता जिस क्षेत्र में हो उसमे ज्ञान का महत्व हम सभी जानते है ।
-
अध्याय : 5 कृष्णभावना भक्ति कर्म का व्यवहारिक ज्ञान
ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते॥ श्लोक 3
हे अर्जुन! जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है क्योंकि राग-द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
व्यवहारिक अर्थ : हे अर्जुन जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी (अपने कर्म या काम मे रमे रहने वाला ) समझने योग्य है क्योंकि राग-द्वेष द्वन्दों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है अगर राग-द्वेष की भावना हो तो ऊर्जा अन्य दिशा में बहती है और लक्ष्य से ध्यान भटकता है ।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ श्लोक 10
जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भाँति पाप से लिप्त नहीं होता ।
व्यवहारिक अर्थ : जो मनुष्य अपने सभी कार्य परमात्मा में अपर्ण करके ये आप करवा रहे है इस भाव के साथ कर्म या अपना काम करता है वह जल से कमल के पत्ते की भाँति पाप से लिप्त नहीं होता ।
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥
श्लोक 19
जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मा में ही स्थित हैं ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में योगेश्वर कहते है जिसका मन या दिमाग समभाव में स्थित है अर्थात एक सा उसने जीवित अवस्था मे ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया है क्योकि सच्चिदाआंनद परमात्मा निर्दोष और सम है, समभाव ये अवस्था कठिन जरूर है पर सम्भव है ।
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्।
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः॥ श्लोक 20
जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरबुद्धि, संशयरहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा में एकीभाव से नित्य स्थित है ।
व्यवहारिक अर्थ : इस श्लोक में योगेश्वर कह रहे है कि जो प्रिय को पाकर खुश अप्रिय को पाकर दुःखी ना हो वह संशय रहित जिसे कोई शंका ना हो वह स्थिरबुद्धि ब्रह्मवेत्ता या ज्ञानी मनुष्य परमात्मा या अपनी उच्च अवस्था सफलता आदि अन्य में स्थित है
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्।